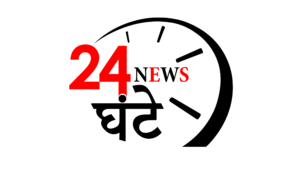सार
बिहार में 1971 के बाद कैसे फिर से एक पार्टी के मुख्यमंत्री का दौर लौटा? इस बदलाव के बावजूद आखिर क्यों राज्य में आठ साल के अंदर पांच मुख्यमंत्री बदल गए? कांग्रेस में फूट का राज्य की सियासत में क्या असर रहा? कैसे बिहार से इसी दौर में शुरू हुई जयप्रकाश नारायण की क्रांति ने पहले कांग्रेस को उखाड़ फेंका और फिर जेपी के नेतृत्व में बना जनता दल खुद ही बिखर गया? आइये जानते हैं…
विस्तार
बिहार में विधानसभा चुनावों और सरकार के बनने-गिरने की कहानी आजादी के बाद से ही काफी दिलचस्प रही है। पहले राज्य में 15 साल तक श्रीकृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में कांग्रेस का एकछत्र राज, फिर पार्टी में ही एक के बाद एक मुख्यमंत्रियों का बदलाव। 1967 के बाद से अलग-अलग राजनीतिक दलों के मुख्यमंत्रियों का शासन और इसके बाद कांग्रेस में ही दो धड़ों के बनने से बिहार में सियासी उथल-पुथल।
अब बारी है बिहार की इससे आगे की राजनीति कहानी। कैसे राज्य में 1971 के बाद फिर से एक पार्टी के मुख्यमंत्री का दौर लौटा? इस बदलाव के बावजूद आखिर क्यों राज्य में आठ साल के अंदर पांच मुख्यमंत्री बदल गए? कांग्रेस में फूट का राज्य की सियासत में क्या असर रहा? कैसे बिहार से इसी दौर में शुरू हुई जयप्रकाश नारायण की क्रांति ने पहले कांग्रेस को उखाड़ फेंका और फिर जेपी के नेतृत्व में बना जनता दल खुद ही बिखर गया? आइये जानते हैं…
1. 1972: लोकसभा से लेकर विधानसभा तक बदली सत्ता की बयार
दिसंबर 1971 में भोला पासवान शास्त्री के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। यह तब हटा, जब बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव का एलान हुआ और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस (आर) को दोनों ही ओर जबरदस्त जीत मिली। बताया जाता है कि बिहार में आम लोग बहु-दलीय सिस्टम और इसकी अस्थिरता से तंग आ गए थे। बार-बार बदलती सत्तासीन पार्टियां और मुख्यमंत्रियों को देखते हुए बिहार ने इस बार निर्णायक स्तर पर वोटिंग की।
1972 में बिहार में 318 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस ने 261 सीटों पर चुनाव लड़ा। पार्टी को 167 सीटों पर जीत मिली। यानी कांग्रेस अपने दम पर ही पूर्ण बहुमत हासिल करने में सफल हो गई। यानी यह तय हो गया कि अगले पांच साल बिहार को स्थिर सरकार मिलेगी। 1969 में हुए मध्यावधि चुनाव में जहां कांग्रेस को 30.12 फीसदी वोट के साथ 118 सीटें मिली थीं, तो वहीं 1972 में उसे 34.12 प्रतिशत वोट मिले थे।
दूसरी तरफ इस चुनाव में क्षेत्रीय दलों को भारी झटका लगा। जिन 20 क्षेत्रीय पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को जोर-शोर से उतारा था, उनमें से नौ का तो सूपड़ा साफ हो गया। हालांकि, निर्दलियों ने अपना किला बचाए रखा और 12 सीटों पर कब्जा जमा लिया।
2. 1973: बिहार को मिला पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री
बिहार में केदार पांडेय की विदाई के बाद कांग्रेस में भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। दरअसल, यहां कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धार्थ शंकर रॉय को सीएम के चुनाव के लिए भेजा। हालांकि, एलएन मिश्र के साथ बैठक के बाद भी पांडेय का उत्तराधिकारी नहीं मिल पाया। एक बार फिर मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार मिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को। उन्होंने इस बार बिहार के नेतृत्व के लिए बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष अब्दुल गफूर को चुना। इस बारे में एलएन मिश्र और केदार पांडेय दोनों को कांग्रेस अध्यक्ष शंकर दयाल शर्मा के घर पर रखी एक बैठक में बता दिया गया।
माना जाता है कि इंदिरा गांधी के गफूर को चुनने की वजह एलएन मिश्र ही थे, जो कि दिल्ली में बैठकर बिहार की राजनीति को उस दौर में नियंत्रित करते थे। दूसरी तरफ केदार पांडेय इस पद पर विधानसभा स्पीकर हरिनाथ मिश्र को चाहते थे। लेकिन उनकी पसंद को अनसुना करते हुए 2 जुलाई 1973 को अब्दुल गफूर को शपथ दिला दी गई। 1967 के बाद से यह 11वीं बार था, जब बिहार में सरकार परिवर्तन हुआ था। यानी महज छह साल में 11वीं बार। इस तरह अब्दुल गफूर बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री और बीपी मंडल के बाद विधान परिषद से आकर सीएम बनने वाले दूसरे नेता बने।